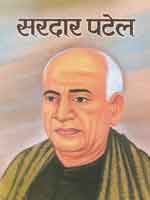|
कविता संग्रह >> दर्द दिया है दर्द दिया हैनीरज
|
49 पाठक हैं |
|||||||
प्रस्तुत है नीरज की कवितायें
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
दृष्टिकोण
जब लिखने के लिए लिखा जाता है तब जो कुछ लिख जाता है उसका नाम है गद्य, पर
जब लिखे बिना न रहा जाए और जो खुद लिख-लिख जाए उसका नाम है कविता। मेरे
जीवन में कविता लिखी नहीं गई, खुद लिख-लिख गई है, ऐसे ही जैसे पहाड़ों पर
निर्झर और फूलों पर ओस की कहानी लिख जाती है। जिस प्रकार जल-जलकर बुझ जाना
दीपक के जीवन की विवशता है। उसी प्रकार गा-गाकर चुप हो जाना मेरे जीवन की
मजबूरी है। मजबूरी यानी वह मेरे अस्तित्व की शर्त है, अनिवार्यता है, और
इसीलिए मैं उसे नहीं वह मुझे बाँधे हुए है। वह मुक्त है और मोक्ष भी, तभी
तो न वह किसी वाद की अनुगामिनी है और न किसी सिद्धान्त की भामिनी। वह मुझ
से ही नहीं दूसरों से भी कहती है-
तुम लिखो हर बात चाहे जिस तरह चाहो,
काव्य को पर वाद का कंगन न बनने दो।
काव्य को पर वाद का कंगन न बनने दो।
क्योंकि वह यह मानती है-
आयु है जितनी समय की गीत की उतनी उमर है,
चाँदनी जब से हँसी है, रागिनी तब से मुखर है,
जिन्दगी गीता स्वयं है जान लें गाना अगर हम,
हर सिसकती साँस लय है, हर छलकता अश्रु स्वर है।
चाँदनी जब से हँसी है, रागिनी तब से मुखर है,
जिन्दगी गीता स्वयं है जान लें गाना अगर हम,
हर सिसकती साँस लय है, हर छलकता अश्रु स्वर है।
उत्तर से दक्खिन, पूरब से पश्चिम और धरती से आकाश तक जो कुछ भी प्रत्यक्ष
या परोक्ष रूप से हमारी प्राण-सत्ता को प्रभावित करता है वह सब कुछ उसका
विषय है-चाहे वह अंधकार हो या प्रकाश, जन्म हो या मृत्यु, सुख हो या दु:ख,
राग हो या विराग, धूप हो या छांह, संघर्ष हो या शान्ति, चाहे वह किसी
प्रवासी की सूनी साँझ हो अथवा किसी संयोगी की सुबह, चाहे वह तपती-जलती हुई
किसी श्रमिक की दोपहर हो अथवा प्रणय-केलि में रत किसी प्रेयसी की चाँदनी
रात। जहाँ तक जीवन है, जहाँ तक सृष्टि है, वहाँ तक उसकी गति है। उसके लिए
कुछ भी त्याज्य नहीं है। अशिव को शिव, असुन्दर को सुन्दर और असत्य को वह
सत्य बनाना चाहती है। यही उसके गाने का ध्येय है और यही उसके रोने का अर्थ
है। उसने शब्दों का जो महल बनाया है उसमें दीवानेखास-जैसी कोई चीज़ नहीं
है। वहाँ केवल दीवानेआम ही है और उसमें प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जाति,
प्रत्येक वर्ण, बिना किसी संकोच के प्रवेश कर सकता है और आमने-सामने खड़ा
होकर अपनी बात कह सकता है। उसके पास सबकी सुनने की सहिष्णुता है, क्योंकि
उसने यह माना है कि सत्य किसी एक की ही थाती नहीं और न ही उसका एक रास्ता
है। वह फुटपाथ पर भूख से छटपटाते हुए एक भिखारी के पास भी मिल सकता है और
वर्षों से अँधेरे में पड़े हुए एक खंडहर में भी, इसीलिए उसने गाया है-
इस द्वार क्यों न जाऊँ,
उस द्वार क्यों न जाऊँ।
घर पा गया तुम्हारा,
मैं घर बदल-बदल कर।
उस द्वार क्यों न जाऊँ।
घर पा गया तुम्हारा,
मैं घर बदल-बदल कर।
मेरी मान्यता है कि साहित्य के लिए मनुष्य से बड़ा और कोई दूसरा सत्य
संसार में नहीं है और उसे पा लेने में ही उसकी सार्थकता है। जो साहित्य
मनुष्य के सुख-दुख का साझीदार नहीं, उससे मेरा विरोध है। मैं अपनी कविता
द्वारा मनुष्य बनकर मनुष्य तक पहुँचना चाहता हूँ। वही मेरी यात्रा का आदि
है, और वही अंत। रास्ते पर कहीं मेरी कविता भटक न जाए, इसलिए उसके हाथ में
मैंने प्रेम का एक दीपक दे दिया है। मानवीय सम्बन्धों में मेरे विचार से
प्रेम सर्वश्रेष्ठ सम्बन्ध है। वह एक ऐसी हृदय साधना है जो निरन्तर हमारी
विकृतियों का शमन करती हुई हमें मनुष्यता के निकट ले जाती है। व्यक्ति के
जीवन की मूल विकृति मैं अहं को मानता हूं, जो सामाजिक रूप में स्वार्थ का
रूप धारण करता है। घृणा, द्वेष, दम्भ, वैषम्य, युद्ध, संहार इन सबका कारण
यही अहं है। इसी से मुक्त होने में मनुष्य की मुक्ति है। मेरी परिभाषा में
इसी अहं के समर्पण का नाम प्रेम है और इसी अहं के विसर्जन का नाम साहित्य
है। जो प्रेम का इष्ट है वही साहित्य का लक्ष्य है, इसीलिए मेरे विचार से
अपने अन्तिम रूप में प्रेम-साधना के समान साहित्य साधना भी हृदय साधना ही
है। कवि बनना है तो पहले महान् मनुष्य बनो-यह मेरे काव्य का शीर्ष वाक्य
है।
तो प्रेम और विशेष रूप से मानव-प्रेमी मेरी कविता का मूल स्वर है। ‘आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूँ,’ यह मेरी कमज़ोरी भी है और शक्ति भी है। कमज़ोरी इसलिए कि घृणा और द्वेष से भरे आज के संसार में मानव-प्रेम के गीत गाना अपनी पराजय की कहानी ही कहना है, पर शक्ति इसलिए है कि मेरे इस मानव-प्रेम ने ही मेरे आसपास बनी हुई धर्म-कर्म, जाति-पाँति आदि की दीवारों को ढहा दिया है और वादों के भीषण झंझावात में भी मुझे पथभ्रष्ट नहीं होने दिया है, जब मैं अपना सत्य खोजने निकला था-
तो प्रेम और विशेष रूप से मानव-प्रेमी मेरी कविता का मूल स्वर है। ‘आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूँ,’ यह मेरी कमज़ोरी भी है और शक्ति भी है। कमज़ोरी इसलिए कि घृणा और द्वेष से भरे आज के संसार में मानव-प्रेम के गीत गाना अपनी पराजय की कहानी ही कहना है, पर शक्ति इसलिए है कि मेरे इस मानव-प्रेम ने ही मेरे आसपास बनी हुई धर्म-कर्म, जाति-पाँति आदि की दीवारों को ढहा दिया है और वादों के भीषण झंझावात में भी मुझे पथभ्रष्ट नहीं होने दिया है, जब मैं अपना सत्य खोजने निकला था-
पर्वतों ने झुका शीश चूमे चरण,
बाँह डाली कली ने गले में चंचल।
एक तस्वीर तेरे लिए किन्तु मैं-
साफ दामन बचाकर गया ही निकल।
बाँह डाली कली ने गले में चंचल।
एक तस्वीर तेरे लिए किन्तु मैं-
साफ दामन बचाकर गया ही निकल।
-प्राण गीत
मेरे पास मनुष्य की तसवीर थी इसीलिए मैं रास्ते में नहीं भटक सका। इसीलिए
यह मेरी शक्ति है। पर इसे पूरी तरह समझने के लिए यह आवश्यक है कि आप यह भी
जान लें कि मुझे इसकी कितने रूपों में अनुभूति हुई है। मैं यह मानता हूँ
कि पेट की भूख के साथ-साथ मनुष्य में एक और भी भूख है, जिसका नाम है सृजन
की भूख। प्रकृति का प्रत्येक तत्त्व जो स्वयं को विश्व में किसी न किसी
रूप में प्रतिबिम्बित करने के लिए विकल है उसका कारण यही है-
दीप को अपना बनाने को
पतंगा जल रहा है,
बूंद बनने को समुन्दर की
हिमालय गल रहा है।
पतंगा जल रहा है,
बूंद बनने को समुन्दर की
हिमालय गल रहा है।
यही सृष्टि की प्रजनन प्रक्रिया है। इसे ही वासना कहा गया है। यही
प्रत्येक कला और साहित्य की मूल प्रेरणा है। यह वासना भिन्न-भिन्न चेतना
स्तरों पर भिन्न-भिन्न रूप धारण करती है। मनुष्य में पंच-कोषों की सत्ता
को मैं व्यक्ति की पंच-चेतनाओं व रूप में स्वीकार करता हूं। निरन्तर
विकासशील होने के कारण कवि के मानस में व्याप्त सृजन की यह भूख सतत
ऊर्ध्वगामी होती है जिसके फलस्वरूप उसे भिन्न-भिन्न प्रकार की अनुभूति
होती है। जब तक यह वासना अन्नमय कोष में व्याप्त रही है, तब तक यह
‘आकर्षण’ कहलाती है। इस स्तर पर मनुष्य मांसलता से
आक्रान्त रहता है और इस समय उसके भीतर का पशु प्रबल होता है। वह पाना तो
चाहता है, किन्तु देना कुछ नहीं चाहता-यही पाशविक वृत्ति है और इसी का नाम
स्वार्थ है। इस स्तर पर जो रचना की जाती है वह घोर यौन-तृष्णा से विकल
होती है। मैंने जीवन में इस प्रकार का केवल एक गीत लिखा है-आज तो मुझसे न
शरमाओ तुम्हें मेरी कसम है। संयम के कारण जब यही वासना और ऊपर की ओर
संक्रमण करती है तब प्राणकोष में प्रवेश करती है। प्राणकोष में पवन यानी
आवागमन है। यहीं से ‘प्रेम’ का उदय होता है। इस स्तर
पर मनुष्य में प्राप्ति की कामना के साथ-साथ देने की भावना भी रहती है।
यहाँ से स्वार्थ का परिहार आरम्भ होता है, पर स्वार्थ की चेतना सर्वथा मिट
जाती नहीं जाती। पशुत्व क्षीण होने लगता है और मनुष्यत्व प्रबल होने लगता
है। पर पूर्णतया उसका विनाश नहीं हो पाता, इसीलिए प्रेम के साथ-साथ
ईर्ष्या भी चलती रहती है। यहीं से काव्य में दार्शनिकता का जन्म होता है।
‘विभावरी’ में संग्रहीत मेरी अधिकांश रचनाएँ इसी स्तर
की हैं और कुछ ‘प्राण-गीत’ की भी। प्राणमय-कोष से जब
यह मनोमय-कोष में गमन करती है तब कवि में ‘भक्ति’ की
अनुभूति जागृत होती है। प्राप्ति की कामना यहाँ सो जाती है। कविता यहाँ
पहुँचकर स्त्री बन जाती है, क्योंकि समर्पण स्त्री ही कर सकती है, पुरुष
नहीं। भक्त कवियों तथा सूफियों ने जो ‘राम की
बहुरिया’ बनकर अपने हृदय की वेदना व्यक्त की है उसका तथा
भारतवर्ष में सखी सम्प्रदाय के जन्म का कारण भी यही है। मेरी भी कुछ
कविताएँ इसी स्तर की हैं। उदाहरणार्थ, यह गीत-
तुझसे लगन लगाई,
उमर भर नींद न आई।
साँस-साँस बन गई सुमिरनी,
मृगछाला सब की सब धरिणी,
क्या गंगा, कैसी वैतरिणी,
भेद न कुछ कर पाई,
दहाई बनी इकाई।
उमर भर नींद न आई।
साँस-साँस बन गई सुमिरनी,
मृगछाला सब की सब धरिणी,
क्या गंगा, कैसी वैतरिणी,
भेद न कुछ कर पाई,
दहाई बनी इकाई।
भक्ति की तन्मयता विरह-वेदना में ही है। विरह का कारण है द्वैत, जिसका
आरम्भ मनोमय कोष से ही होता है। इसीलिए प्रत्येक भक्त कवि ने मोक्ष पर धूल
फेंकी है और अद्वैतवाद को नीरस ज्ञान के रूप में तिरस्कृत किया है।
मनोमय-कोष के ऊपर विज्ञानमय कोष है। यहाँ से द्वैत की समाप्ति आरम्भ होती
है। इस स्तर पर कवि में सामाजिक चेतना और जन-मंगल की भावना जागृत होती है।
यहीं से वास्तविक प्रगतिशील कविता का जन्म होता है। (किन्तु आज की
प्रगतिशील कविता इस श्रेणी में नहीं आती, क्योंकि उसमें से अधिकांश
अनुभूतिशून्य हैं और केवल सिद्धान्त-प्रतिपादन के लिए लिखी सी जान पड़ती
हैं। हाँ, प्रेमचन्द के उपन्यासों में इसके अवश्य दर्शन होते हैं और
कहीं-कहीं नाजिम हिकमत की कविताओं में भी इसकी झलक मिलती है।) मेरी
‘अब युद्ध नहीं होगा’ शीर्षक कविता इसी चेतना-स्तर की
कविता है। यहाँ व्यक्ति न स्त्री-रूप में सोचता है, न पुरुष-रूप में। वह
विश्व का एक अंश बन जाता है। निम्नलिखित गीत में इसी की ध्वनि है-
अँधियारा जिससे शरमाए
उजियारा जिसको ललचाए,
ऐसा दे दो दर्द मुझे तुम
मेरा गीत दिया बन जाए।
उजियारा जिसको ललचाए,
ऐसा दे दो दर्द मुझे तुम
मेरा गीत दिया बन जाए।
और सबसे ऊपर आनन्दमय कोष है। यहाँ अहं का पूर्ण विसर्जन है और प्रेम की यह
अन्तिम परिणति है। यहाँ व्यक्ति की चेतना का विश्व-चेतना में पूर्ण
तिरोभाव है। यही साहित्य का और प्रगतिवाद का अन्तिम सोपान है। गोस्वामी जी
के ‘रामचरितमानस’ में इसी चेतना स्तर की झलक है।
इसी सम्बन्ध में एक बात और कह दूँ। मेरे विचार से अनुभूति का अर्थ है उष्णता (ताप यानी वेदना)। उष्णता (ताप) ही जीवन है। प्रेम की गहराई ताप की अधिकता या न्यूनता से ही नापी जाती है। काव्य में जो मर्मस्पर्शिता होती है उसकी जन्मदात्री भी यही उष्णता या वेदना है। यदि वह नहीं है तो कविता उपदेश भले हो, कविता नहीं कही जा सकती। इसका एक सृजनात्मक पहलू यह है कि यह मनुष्य के हृदय को छूकर उसे सहिष्णु और विशाल बना देती है। सुख आदमी को कैसे सीमित करता है और दु:ख उसे कैसे विस्तृत करता है इस बात को मैंने इस प्रकार कहा है-
इसी सम्बन्ध में एक बात और कह दूँ। मेरे विचार से अनुभूति का अर्थ है उष्णता (ताप यानी वेदना)। उष्णता (ताप) ही जीवन है। प्रेम की गहराई ताप की अधिकता या न्यूनता से ही नापी जाती है। काव्य में जो मर्मस्पर्शिता होती है उसकी जन्मदात्री भी यही उष्णता या वेदना है। यदि वह नहीं है तो कविता उपदेश भले हो, कविता नहीं कही जा सकती। इसका एक सृजनात्मक पहलू यह है कि यह मनुष्य के हृदय को छूकर उसे सहिष्णु और विशाल बना देती है। सुख आदमी को कैसे सीमित करता है और दु:ख उसे कैसे विस्तृत करता है इस बात को मैंने इस प्रकार कहा है-
मैंने तो चाहा बहुत कि अपने घर में रहूँ अकेला पर,
सुख ने दरवाजा बन्द किया, दुख ने दरवाजा खोल दिया।
सुख ने दरवाजा बन्द किया, दुख ने दरवाजा खोल दिया।
मेरी कविताओं में इसी वेदना (उष्णता) की सहज स्वीकृति है। कुछ लोगों के
विचार से यह नैराश्य-प्रसूत है, पर मेरे अपने अनुभव से यह अपनी
काव्य-वस्तु के प्रति मेरी निश्छल एवं एकान्तिक तन्मयता के कारण ही है।
इसे आप यदि मेरी कविताओं से निकाल देंगे तो मेरी उमर आधी रह जाएगी। मैं ही
क्या संसार में जितने महान कवि हुए हैं उनकी रचनाओं से यदि आप उनकी वेदना
को बहिष्कृत कर दें तो फिर शायद आप ही उन्हें पढ़ना पसन्द नहीं करेंगे।
कविता के आन्तरिक संगठन के विषय में मेरा मत है कि यद्यपि श्रेष्ठ कविता में हृदय और बुद्धि का सन्तुलन होता है, तथापि उनकी क्रियाएँ विपरीत होती हैं। बु्द्धि का कार्य सोचना है और हृदय का व्यापार अनुभूति प्राप्त करना है। कविता में दोनों की क्रियाएँ बदल जाती हैं। हृदय सोचने लगता है और बुद्धि अनुभव करने लगती है। इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि कविता में बुद्धि सोचती तो है, पर हृदय के माध्यम से ही सोचती है। बाइबिल में एक वाक्य है-In the beginning was, word, and word was God-’ आदि में शब्द था और शब्द ईश्वर था।’ शब्द का अर्थ है प्रतीक। प्रतीक का अर्थ है विचार और ईश्वर का अर्थ है सृष्टि यानी विचार सृष्टि है। कविता भी एक सृष्टि है, पर वहाँ विचार को नहीं केवल भाव को ही स्थान है (कविता सुनकर लोग कहते हैं आपका भाव बहुत सुन्दर है आपका विचार सुन्दर है यह कोई नहीं कहता। पर विचार ही वहाँ भाव बन जाता है। कैसे ? बाइबिल का ही एक दूसरा वाक्य है-All was water and a spirit was brooding over it-’ सब ओर जल था और उस पर एक चेतना मनन कर रही थी।’ ‘मनन’ शब्द ‘ब्रूडिंग’ के लिए आया है। ‘ब्रूडिंग’ का अर्थ सेना भी होता है। मुर्गी जब अपने अण्डे को सेती है तो उसके द्रव्य-तत्त्व में प्राण-संचार (ताप-संचार) होता है। इसी प्रकार जब कवि किसी विचार पर मनन करता है, उसे सेता है यानी जब उसमें सम्पूर्ण व्यक्तित्व को डूबो देता है, जैसे मुर्गी अपने तन-मन-प्राण-पंख सबके ताप को केन्द्रित कर अण्डे के द्रव्य में संचरित कर देती है तब वह विचार सृष्टि यानी भाव बन जाता है। इसी बात को यदि यों कहें तो अधिक उपयुक्त होगा-‘जब तक हम किसी विचार को आत्मसात् किए रहते हैं तब तक वह विचार विचार रहता है, किन्तु जब विचार हमें आत्मसात् कर लेता है यानी हमारे सम्पूर्ण व्यक्तित्व-तन, मन, रक्त, मांस, मज्जा आदि में घुल-मिल जाता है तब भाव बन जाता है।’ मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जिन कविताओं को मैंने प्रतीक्षा करने के बाद लिखा है वे मेरी श्रेष्ठ रचनाएँ हुई हैं।
कोई भी विचार एक बार मन में उठकर कभी मिट नहीं पाता ! वह हमारी उपचेतना में चला जाता है और कुछ काल बाद एक तीव्र अनुभूति के रूप में हमारे कंठ से फूट पड़ता है। यह जो फूटना है वही सहज है और वही कविता है। गीत की रचना में हमें कविता से एक कदम और आगे बढ़ना पड़ता है। उसकी सृष्टि में बुद्धि पूर्णतया हृदय की शरण में जाकर सोचने का कार्य कंठ को सौंप देती है। ऐसा इसलिए होता है कि गीत का प्राण केवल एक अमूर्त भाव होता है जो स्वर-संकेत से व्यक्त होता है। जब तक रचना का आधार मूर्त होता है तभी तक बुद्धि साथ देती है, किन्तु जैसे ही विषय अमूर्त हुआ बुद्धि निस्सम्बल होकर हृदय के पास जाकर समर्पण कर देती है। कविता में हम हृदय से सोचते हैं और बुद्धि (विवेक) से अनुभूति प्राप्त करते हैं, किन्तु गीत में हृदय कंठ के द्वारा सोचने लगता है। इसलिए बिना गुनगुनाए हुए गीत नहीं लिखा जाता। यह क्रिया इतनी सूक्ष्म होती है कि कभी-कभी ही रचना के क्षणों में इसका आभाव होता है।
मेरी भाषा के प्रति लोगों की शिकायत रही है कि न तो वह हिन्दी है और न उर्दू। उनकी यह शिकायत सही है और इसका कारण यह है कि मेरे काव्य का जो विषय ‘मानव-प्रेम’ है उसकी भाषा भी इन दोनों में से कोई नहीं है। हृदय में प्रेम सहज ही अंकुरित होता है और वह जीवन में सहज ही हमें प्राप्त होता है। जो सहज है उसके लिए सहज भाषा ही अपेक्षित है। असहज भाषा में यदि वह कहा जाएगा तो अनकहा ही रह जाएगा। प्रत्येक समाज की एक सहज भाषा होती है। मैं जिस समाज में रहता हूँ उस समाज की सहज भाषा वही है जिसमें मैं कविता लिखता हूँ। जो विषय असहज हैं उनके लिए मैंने भी असहज भाषा का ही प्रयोग किया है, जैसे ‘स्रष्टा’, ‘जीवन-गीत’ अरविन्द की कविताओं के अनुवाद आदि। फिर मैं यह भी मानता हूँ कि प्रत्येक विषय की भाषा अलग होती है। चेतना के पंचस्तरों के साथ-ही-साथ भाषा के भी-चिह्न, संकेत, भाव, सूत्र और मंत्र पाँच स्तर होते हैं-चिह्न (आकर्षण), संकेत (प्रेम), भाव (भक्ति), सूत्र (अंशरूप), मंत्र (आनन्द)। विषय के अनुरूप मैंने भी चित्रमयी, संगीतमयी, परुष, दार्शनिक, सहज, सांकेतिक आदि भाषाओं का प्रयोग किया है। विस्तार-भय से मैं यहाँ उद्धरण नहीं दे रहा हूँ किन्तु यदि आप ध्यान से मेरी रचनाओं को पढ़ेंगे तो आपको इन सबके उदाहरण उनमें मिल जाएँगे।
मैंने कविताओं की अपेक्षा गीत अधिक लिखे हैं और मेरे गीत लोकप्रिय भी हुए हैं-यह भी सत्य है। अधिकांश लोग उनकी लोकप्रियता का श्रेय मेरे कविता-पाठ के ढंग को देते हैं। कुछ हद तक यह भी सत्य है, पर उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा काम है उनकी निर्झर सी अबाध गति और स्वाभाविक भाषा में गुंथी हुई स्वाभाविक अनुभूति। कविता की सबसे बड़ी शक्ति उसकी गति और स्वाभाविकता ही है। जब हम स्वाभाविकता से अस्वाभाविकता की ओर जाते हैं तब गद्य रचना करते हैं और जब अस्वाभाविकता से स्वाभाविकता की ओर जाते हैं तब कविता लिखते हैं। स्वाभाविकता ही गति है, जो व्यष्टि, समष्टि और सृष्टि सबकी स्थिति का एकमात्र कारण है। कविता भी एक सृष्टि है, इसलिए सृष्टि के समान गति (लय) उसकी भी आधारशिला है। वाक्य में गति क्रिया के सहज एवं उचित प्रयोग से ही आती है। संस्कृत साहित्य उत्तराधिकार में पाने तथा स्वभाव से आध्यात्मिक चिन्तन में लीन होने के कारण हिन्दी ने ‘क्रिया’ के महत्त्व को कभी ठीक तरह से नहीं समझा। (ब्रजभाषा और अवधि के कवियों ने यह गलती नहीं की)। या तो उसने उसका बहिष्कार किया या उसका गलत प्रयोग किया। आधुनिक हिन्दी कविता में क्रिया को स्थानच्युत और पदच्युत करने के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। आरम्भ में मैंने भी यही भूल की थी पर एक दिन अचानक ही एक चार वर्ष के बच्चे ने मुझे मेरी भूल सुझाई और तब से मैं क्रिया के प्रयोग के विषय में अधिक सजग रहने लगा। श्रेष्ठ कविता का एक गुण स्मरणीयता भी है और वह भी बहुत कुछ क्रिया के उचित या अनुचित प्रयोग पर ही निर्भर है। जिस वाक्य में ‘क्रिया’ स्थान भ्रष्ट होगी वह वाक्य प्रयत्न करने पर भी स्मृति में अधिक देर तक नहीं ठहर सकता और जिस वाक्य में ‘क्रिया’ अपने निश्चित स्थान पर होगी वह वाक्य बिना प्रयास हमारे स्मृति-पट पर अंकित हो जाएगा। नीचे के दो उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाएगा-
कविता के आन्तरिक संगठन के विषय में मेरा मत है कि यद्यपि श्रेष्ठ कविता में हृदय और बुद्धि का सन्तुलन होता है, तथापि उनकी क्रियाएँ विपरीत होती हैं। बु्द्धि का कार्य सोचना है और हृदय का व्यापार अनुभूति प्राप्त करना है। कविता में दोनों की क्रियाएँ बदल जाती हैं। हृदय सोचने लगता है और बुद्धि अनुभव करने लगती है। इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि कविता में बुद्धि सोचती तो है, पर हृदय के माध्यम से ही सोचती है। बाइबिल में एक वाक्य है-In the beginning was, word, and word was God-’ आदि में शब्द था और शब्द ईश्वर था।’ शब्द का अर्थ है प्रतीक। प्रतीक का अर्थ है विचार और ईश्वर का अर्थ है सृष्टि यानी विचार सृष्टि है। कविता भी एक सृष्टि है, पर वहाँ विचार को नहीं केवल भाव को ही स्थान है (कविता सुनकर लोग कहते हैं आपका भाव बहुत सुन्दर है आपका विचार सुन्दर है यह कोई नहीं कहता। पर विचार ही वहाँ भाव बन जाता है। कैसे ? बाइबिल का ही एक दूसरा वाक्य है-All was water and a spirit was brooding over it-’ सब ओर जल था और उस पर एक चेतना मनन कर रही थी।’ ‘मनन’ शब्द ‘ब्रूडिंग’ के लिए आया है। ‘ब्रूडिंग’ का अर्थ सेना भी होता है। मुर्गी जब अपने अण्डे को सेती है तो उसके द्रव्य-तत्त्व में प्राण-संचार (ताप-संचार) होता है। इसी प्रकार जब कवि किसी विचार पर मनन करता है, उसे सेता है यानी जब उसमें सम्पूर्ण व्यक्तित्व को डूबो देता है, जैसे मुर्गी अपने तन-मन-प्राण-पंख सबके ताप को केन्द्रित कर अण्डे के द्रव्य में संचरित कर देती है तब वह विचार सृष्टि यानी भाव बन जाता है। इसी बात को यदि यों कहें तो अधिक उपयुक्त होगा-‘जब तक हम किसी विचार को आत्मसात् किए रहते हैं तब तक वह विचार विचार रहता है, किन्तु जब विचार हमें आत्मसात् कर लेता है यानी हमारे सम्पूर्ण व्यक्तित्व-तन, मन, रक्त, मांस, मज्जा आदि में घुल-मिल जाता है तब भाव बन जाता है।’ मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जिन कविताओं को मैंने प्रतीक्षा करने के बाद लिखा है वे मेरी श्रेष्ठ रचनाएँ हुई हैं।
कोई भी विचार एक बार मन में उठकर कभी मिट नहीं पाता ! वह हमारी उपचेतना में चला जाता है और कुछ काल बाद एक तीव्र अनुभूति के रूप में हमारे कंठ से फूट पड़ता है। यह जो फूटना है वही सहज है और वही कविता है। गीत की रचना में हमें कविता से एक कदम और आगे बढ़ना पड़ता है। उसकी सृष्टि में बुद्धि पूर्णतया हृदय की शरण में जाकर सोचने का कार्य कंठ को सौंप देती है। ऐसा इसलिए होता है कि गीत का प्राण केवल एक अमूर्त भाव होता है जो स्वर-संकेत से व्यक्त होता है। जब तक रचना का आधार मूर्त होता है तभी तक बुद्धि साथ देती है, किन्तु जैसे ही विषय अमूर्त हुआ बुद्धि निस्सम्बल होकर हृदय के पास जाकर समर्पण कर देती है। कविता में हम हृदय से सोचते हैं और बुद्धि (विवेक) से अनुभूति प्राप्त करते हैं, किन्तु गीत में हृदय कंठ के द्वारा सोचने लगता है। इसलिए बिना गुनगुनाए हुए गीत नहीं लिखा जाता। यह क्रिया इतनी सूक्ष्म होती है कि कभी-कभी ही रचना के क्षणों में इसका आभाव होता है।
मेरी भाषा के प्रति लोगों की शिकायत रही है कि न तो वह हिन्दी है और न उर्दू। उनकी यह शिकायत सही है और इसका कारण यह है कि मेरे काव्य का जो विषय ‘मानव-प्रेम’ है उसकी भाषा भी इन दोनों में से कोई नहीं है। हृदय में प्रेम सहज ही अंकुरित होता है और वह जीवन में सहज ही हमें प्राप्त होता है। जो सहज है उसके लिए सहज भाषा ही अपेक्षित है। असहज भाषा में यदि वह कहा जाएगा तो अनकहा ही रह जाएगा। प्रत्येक समाज की एक सहज भाषा होती है। मैं जिस समाज में रहता हूँ उस समाज की सहज भाषा वही है जिसमें मैं कविता लिखता हूँ। जो विषय असहज हैं उनके लिए मैंने भी असहज भाषा का ही प्रयोग किया है, जैसे ‘स्रष्टा’, ‘जीवन-गीत’ अरविन्द की कविताओं के अनुवाद आदि। फिर मैं यह भी मानता हूँ कि प्रत्येक विषय की भाषा अलग होती है। चेतना के पंचस्तरों के साथ-ही-साथ भाषा के भी-चिह्न, संकेत, भाव, सूत्र और मंत्र पाँच स्तर होते हैं-चिह्न (आकर्षण), संकेत (प्रेम), भाव (भक्ति), सूत्र (अंशरूप), मंत्र (आनन्द)। विषय के अनुरूप मैंने भी चित्रमयी, संगीतमयी, परुष, दार्शनिक, सहज, सांकेतिक आदि भाषाओं का प्रयोग किया है। विस्तार-भय से मैं यहाँ उद्धरण नहीं दे रहा हूँ किन्तु यदि आप ध्यान से मेरी रचनाओं को पढ़ेंगे तो आपको इन सबके उदाहरण उनमें मिल जाएँगे।
मैंने कविताओं की अपेक्षा गीत अधिक लिखे हैं और मेरे गीत लोकप्रिय भी हुए हैं-यह भी सत्य है। अधिकांश लोग उनकी लोकप्रियता का श्रेय मेरे कविता-पाठ के ढंग को देते हैं। कुछ हद तक यह भी सत्य है, पर उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा काम है उनकी निर्झर सी अबाध गति और स्वाभाविक भाषा में गुंथी हुई स्वाभाविक अनुभूति। कविता की सबसे बड़ी शक्ति उसकी गति और स्वाभाविकता ही है। जब हम स्वाभाविकता से अस्वाभाविकता की ओर जाते हैं तब गद्य रचना करते हैं और जब अस्वाभाविकता से स्वाभाविकता की ओर जाते हैं तब कविता लिखते हैं। स्वाभाविकता ही गति है, जो व्यष्टि, समष्टि और सृष्टि सबकी स्थिति का एकमात्र कारण है। कविता भी एक सृष्टि है, इसलिए सृष्टि के समान गति (लय) उसकी भी आधारशिला है। वाक्य में गति क्रिया के सहज एवं उचित प्रयोग से ही आती है। संस्कृत साहित्य उत्तराधिकार में पाने तथा स्वभाव से आध्यात्मिक चिन्तन में लीन होने के कारण हिन्दी ने ‘क्रिया’ के महत्त्व को कभी ठीक तरह से नहीं समझा। (ब्रजभाषा और अवधि के कवियों ने यह गलती नहीं की)। या तो उसने उसका बहिष्कार किया या उसका गलत प्रयोग किया। आधुनिक हिन्दी कविता में क्रिया को स्थानच्युत और पदच्युत करने के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। आरम्भ में मैंने भी यही भूल की थी पर एक दिन अचानक ही एक चार वर्ष के बच्चे ने मुझे मेरी भूल सुझाई और तब से मैं क्रिया के प्रयोग के विषय में अधिक सजग रहने लगा। श्रेष्ठ कविता का एक गुण स्मरणीयता भी है और वह भी बहुत कुछ क्रिया के उचित या अनुचित प्रयोग पर ही निर्भर है। जिस वाक्य में ‘क्रिया’ स्थान भ्रष्ट होगी वह वाक्य प्रयत्न करने पर भी स्मृति में अधिक देर तक नहीं ठहर सकता और जिस वाक्य में ‘क्रिया’ अपने निश्चित स्थान पर होगी वह वाक्य बिना प्रयास हमारे स्मृति-पट पर अंकित हो जाएगा। नीचे के दो उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाएगा-
आज जी भर देख लो तुम चाँद को,
क्या पता यह रात फिर आए न आए।
एक तिनके से किसी तूफान के-
साथ उड़कर जब लिया आकाश छू।
क्या पता यह रात फिर आए न आए।
एक तिनके से किसी तूफान के-
साथ उड़कर जब लिया आकाश छू।
ऊपर दिए हुए दोनों उदाहरणों में जो अन्तर है वह स्पष्ट है। पहले वाक्य में
क्रिया अपने यथास्थान पर है, इसलिए गति के साथ-साथ उसकी स्मरणीयता भी बढ़
जाती है। दूसरे स्थान में ‘छू लिया’ को तोड़कर उसे
स्थानच्युत कर दिया गया है, इसलिए वाक्य की स्मरणयीता नहीं, उसकी गति भी
क्षीण हो जाती है।
भाषा, अर्थ और संकेत की स्वाभाविकता में शब्द का महत्त्वपूर्ण स्थान है। अकेले शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। शब्द का अर्थ वाक्य अर्थात् अन्य शब्दों के सम्बन्ध तथा समय और स्थान के सन्दर्भ से प्राप्त होता है। मैंने यह माना है कि जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य अपूर्ण है और उसे पूर्णता देने वाला उसकी आत्मा का साथी इस संसार में कहीं छुपा है उसी प्रकार प्रत्येक शब्द भी अपूर्ण है और उसका भी एक पूरक शब्द है-जैसे सुबह का शाम, जमीन का आसमान, दिन का रात आदि-आदि। जिस ध्वनि-सामंजस्य के फलस्वरूप एक शब्द का सम्बन्ध दूसरे से जुड़ता है वह शताब्दियों के प्रयोग और संस्कार के बाद प्राप्त होता है, क्योंकि भाषा व्यक्ति की नहीं, समाज की सृष्टि है। कोश में प्रत्येक शब्द के कुछ न कुछ पर्यायवाची शब्द होते हैं, पर कविता के लिए वे नहीं बने हैं। कविता में एक शब्द का स्थान उसी अर्थ का दूसरा शब्द नहीं ले सकता-यदि ले सकता है तो मेरी दृष्टि में यह एक कविता की कमी है। कविता की स्वाभाविक भाषा वह होती है जिसमें प्रत्येक शब्द, दूसरे शब्द का पूरक बनकर उपस्थित हो जैसे निम्नलिखित चरम में-
भाषा, अर्थ और संकेत की स्वाभाविकता में शब्द का महत्त्वपूर्ण स्थान है। अकेले शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। शब्द का अर्थ वाक्य अर्थात् अन्य शब्दों के सम्बन्ध तथा समय और स्थान के सन्दर्भ से प्राप्त होता है। मैंने यह माना है कि जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य अपूर्ण है और उसे पूर्णता देने वाला उसकी आत्मा का साथी इस संसार में कहीं छुपा है उसी प्रकार प्रत्येक शब्द भी अपूर्ण है और उसका भी एक पूरक शब्द है-जैसे सुबह का शाम, जमीन का आसमान, दिन का रात आदि-आदि। जिस ध्वनि-सामंजस्य के फलस्वरूप एक शब्द का सम्बन्ध दूसरे से जुड़ता है वह शताब्दियों के प्रयोग और संस्कार के बाद प्राप्त होता है, क्योंकि भाषा व्यक्ति की नहीं, समाज की सृष्टि है। कोश में प्रत्येक शब्द के कुछ न कुछ पर्यायवाची शब्द होते हैं, पर कविता के लिए वे नहीं बने हैं। कविता में एक शब्द का स्थान उसी अर्थ का दूसरा शब्द नहीं ले सकता-यदि ले सकता है तो मेरी दृष्टि में यह एक कविता की कमी है। कविता की स्वाभाविक भाषा वह होती है जिसमें प्रत्येक शब्द, दूसरे शब्द का पूरक बनकर उपस्थित हो जैसे निम्नलिखित चरम में-
अनजान यह नगर है, अनजान यह डगर है।
न चढ़ाव का पता है, न ढलाव की खबर है।
सब कह रहे मुसाफिर ! चलना सँभल-सँभलकर।
लम्बा बहुत सफर है, छोटी बहुत उमर है।
न चढ़ाव का पता है, न ढलाव की खबर है।
सब कह रहे मुसाफिर ! चलना सँभल-सँभलकर।
लम्बा बहुत सफर है, छोटी बहुत उमर है।
इस प्रकार की भाषा से जो संगीत उत्पन्न होता है वह स्वर-संगीत शब्द-संगीत
आदि ये बढ़कर हृदय-संगीत होता है और यही संगीत भाव-संगीत के रूप में गीत
का इष्ट होता है। मेरे गीतों में अन्त:सलिला के समान यही संगीत व्याप्त
है। चेतना के जिस स्तर पर ‘भक्ति’ का उदय होता है उसी
स्तर पर इस संगीत का जन्म होता है। सूर, मीरा, महादेवी और कोकिलजी की इधर
की रचनाओं में यह व्याप्त है। बच्चनजी की भी कुछ रचनाओं में हमें इसके
दर्शन होते हैं।
यह रही मेरी बात ! प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तथा अन्य वादों के रूप में जो विवाद आज हिन्दी में प्रचलित है उनमें मेरी आस्था नहीं है। यद्यपि मैं प्रगति को जीवन का इष्ट मानता हूं और प्रयोग को प्रगति का सहायक, किन्तु न तो किसी वाद-विशेष से आक्रान्त प्रगति का मैं पोषक हूं और न किसी सिद्धान्त-विशेष से सम्बन्धित प्रयोग का हिमायती। जीवन के वाक्य पर विराम-चिह्न नहीं रखा जा सकता, उसको बाँध देना उसकी गति को अवरूद्ध कर देना है। साहित्य जीवन का उपनाम है। मेरी दृष्टि में वही साहित्य श्रेष्ठ है जो हमें हमारे व्यक्तित्व के संकुचित घेरे से निकालकर अधिक-से-अधिक विश्व-मानवता के निकट ले जाता है। वास्तविक प्रयोग मेरे निकट वह है जो विचार-प्रयोग के साथ-साथ भाषा, छन्द, लय, तान आदि के भी प्रयोग करता है। विचार-प्रयोग को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के प्रयोग मेरे विचार से फैशन हैं और वे पेरिस की सड़कों पर ही प्रतिष्ठा पा सकते हैं, वृन्दावन या अयोध्या की गलियों में नहीं। यहाँ तो सूर-मीरा की तन्मयता और तुलसी का जीवन दर्शन ही अपेक्षित है ! और फिर ऐसा हृदय जो कह सके-
यह रही मेरी बात ! प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तथा अन्य वादों के रूप में जो विवाद आज हिन्दी में प्रचलित है उनमें मेरी आस्था नहीं है। यद्यपि मैं प्रगति को जीवन का इष्ट मानता हूं और प्रयोग को प्रगति का सहायक, किन्तु न तो किसी वाद-विशेष से आक्रान्त प्रगति का मैं पोषक हूं और न किसी सिद्धान्त-विशेष से सम्बन्धित प्रयोग का हिमायती। जीवन के वाक्य पर विराम-चिह्न नहीं रखा जा सकता, उसको बाँध देना उसकी गति को अवरूद्ध कर देना है। साहित्य जीवन का उपनाम है। मेरी दृष्टि में वही साहित्य श्रेष्ठ है जो हमें हमारे व्यक्तित्व के संकुचित घेरे से निकालकर अधिक-से-अधिक विश्व-मानवता के निकट ले जाता है। वास्तविक प्रयोग मेरे निकट वह है जो विचार-प्रयोग के साथ-साथ भाषा, छन्द, लय, तान आदि के भी प्रयोग करता है। विचार-प्रयोग को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के प्रयोग मेरे विचार से फैशन हैं और वे पेरिस की सड़कों पर ही प्रतिष्ठा पा सकते हैं, वृन्दावन या अयोध्या की गलियों में नहीं। यहाँ तो सूर-मीरा की तन्मयता और तुलसी का जीवन दर्शन ही अपेक्षित है ! और फिर ऐसा हृदय जो कह सके-
कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है।
-नीरज
दर्द दिया है
1
दर्द दिया है, अश्रु स्नेह है, बाती बैरिन श्वास है,
जल-जलकर बुझ जाऊँ, मेरा बस इतना इतिहास है !
मैं ज्वाला का ज्योति-काव्य
चिनगारी जिसकी भाषा,
किसी निठुर की एक फूँक का
हूँ बस खेल-तमाशा
पग-तल लेटी निशा, भाल पर
बैठी ऊषा गोरी,
एक जलन से बाँध रखी है
साँझ-सुबह की डोरी
सोये चाँद-सितारे, भू-नभ, दिशि-दिशि स्वप्न-मगन है
पी-पीकर निज आग जग रही केवल मेरी प्यास है !
जल-जलकर बुझ जाऊँ, मेरा बस इतना इतिहास है !!
जल-जलकर बुझ जाऊँ, मेरा बस इतना इतिहास है !
मैं ज्वाला का ज्योति-काव्य
चिनगारी जिसकी भाषा,
किसी निठुर की एक फूँक का
हूँ बस खेल-तमाशा
पग-तल लेटी निशा, भाल पर
बैठी ऊषा गोरी,
एक जलन से बाँध रखी है
साँझ-सुबह की डोरी
सोये चाँद-सितारे, भू-नभ, दिशि-दिशि स्वप्न-मगन है
पी-पीकर निज आग जग रही केवल मेरी प्यास है !
जल-जलकर बुझ जाऊँ, मेरा बस इतना इतिहास है !!
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i